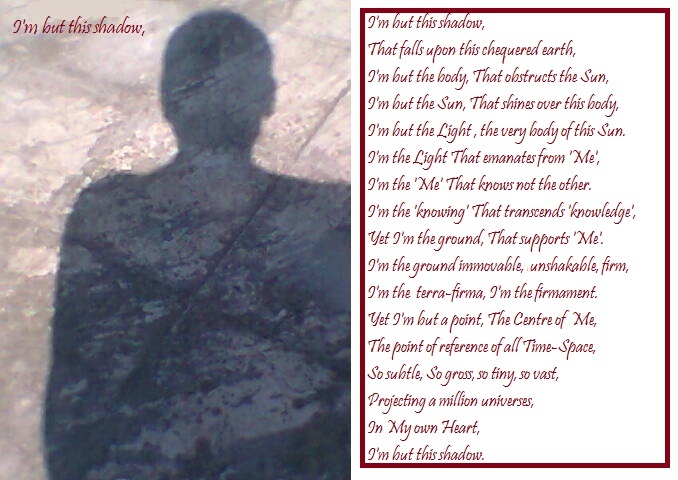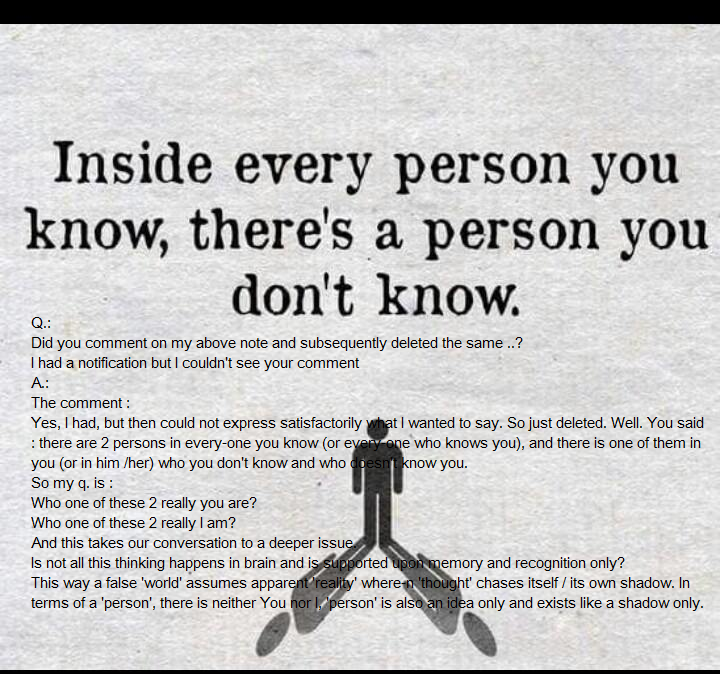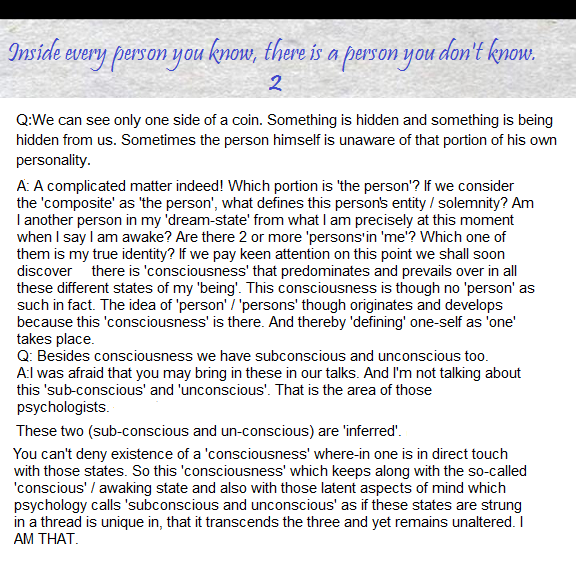The barbed tree-guard.
--
Dear You!,
When I had shifted to my new rented house, there was a beautiful tree along the road-side. I saw it was not safe, and cows, goats or other people could also destroy it. I put a tree-guard and when it was mature and grown up enough to look after itself, the tree-guard was no more needed. Even the barbed fence in the tree-guard could harm the tree.
Then I decided that it is wise to remove the tree-guard. Still it is a bit unsafe, but I think I can't do anything anymore to save it from the possible dangers it might come across in its life.
Just hope Shiva will take care of, look after it.
Then again, I felt if Narayan could not save Narayan Himself, how I could possibly save the tree?
May be it will not be possible for me to keep in touch with you any more, and it matters not.
All the best.
Your own old remembrance.
--
Dear You!,
When I had shifted to my new rented house, there was a beautiful tree along the road-side. I saw it was not safe, and cows, goats or other people could also destroy it. I put a tree-guard and when it was mature and grown up enough to look after itself, the tree-guard was no more needed. Even the barbed fence in the tree-guard could harm the tree.
Then I decided that it is wise to remove the tree-guard. Still it is a bit unsafe, but I think I can't do anything anymore to save it from the possible dangers it might come across in its life.
Just hope Shiva will take care of, look after it.
Then again, I felt if Narayan could not save Narayan Himself, how I could possibly save the tree?
May be it will not be possible for me to keep in touch with you any more, and it matters not.
All the best.
Your own old remembrance.